मैं अक्सर आत्मविस्मृत होकर मुग्ध भाव से तुम्हें देखती रहती, पर मनु इसी भोली प्रक्रिया में एक दिन तुम्हारी आंखों का रंग बदलने लगा था. चाय पीते-पीते उनमें मदिर डोरे तैरने लगे थे और तुम्हारी दृष्टि ने मुझे भीतर तक खींच लिया था. तुम्हारे होंठों की थिरकन कोई रस खींचने के लिए बेताब हो उठी थी और मैं जबरन बांह छुड़ाकर वहां से भाग गई थी. तुम्हारे आहत दर्प को यह गवारा न हुआ और ताव खाया पौरुष फनफनाकर दरवाज़े के बाहर हो गया था.
तेज झोंका कमरे में घुस आया और मेज पर बिखरे सारे काग़ज़ फ़र्र-फ़र्र उड़ने लगे. हवा ने मेरी तन्द्रा भंग कर दी थी. काग़ज़ों को समेटने के लिए मैंने हाथ का पेन बंद कर एक ओर रखा. तभी उठते हुए मेरी नज़र हल्के हरे रंग के ख़ूबसूरत पन्नों पर पड़ी. उन्हें हाथ में लेते ही नन्हे-नन्हें ख़ूबसूरत से अक्षर ढेर सारी ख़ूबसूरत कविताओं में बदल गए और मुझे लगा अचानक मौसम में ठंडी खुनक भर गई है. मेरे मन प्राणों पर एक गर्म सी भाप कोहरा बन लिपटती चली जा रही है.
आज इतने वर्षों के बाद इतनी दूर अपने अपार्टमेन्ट में अकेली बैठी मैं बहुत पीछे लौट गई हूं. बड़ी-बड़ी कांच की खिड़कियों पर लहराते सफ़ेद रेशमी पदों की झालरों के पोछे एक और नीलू बर्फ़ पर सहमी सी खड़ी है अपने आप से अनजान, सहमी सिमटी सी. हां, वहीं नीलू जिसे पहले पहल तुम्हीं ने नीलिमा की पहचान दी थी. अपने आप की पहचान.
सच तो यह है कि आज की यह नीलिमा, अमेरिका के एक बड़े नगर के एक बड़े कॉलेज की दर्शन की प्रोफेसर इसे तुमने ही तो गढ़ा था. पत्थर की अनगढ़ मूर्ति को तराश-तराश कर उसमें ऊष्म स्पंदन भर दिए थे और वह सचमुच अपनी ही नज़र में अपूर्व गर्वमयी बन गई थी. कितने प्यारे थे वे दिन जब उसके हर वेश-परिवेश को एक सोंधी नज़र मिल गई थी. चेहरे की मुस्कुराहट को एक मिठास मिल गई थी. आंधी, तूफ़ान और बर्फीले दिनों को एक सुखद, चटक सुहानी धूप मिल गई थी.
इतने दिनों में एक दिन भी तो ऐसा नहीं लगा कि मैं अकेली हूं. हर पल, हर क्षण तुम्हारी बातें और तुम्हारी मुद्राएं मेरी आंखों में ऊंचे-ऊंचे सपने बन तैरा करती हैं. पर इधर कुछ दिनों से मैंने लोरी गाकर, थपकियां देकर ज़बरदस्ती तुम्हारे साये को सुला रखा था, लेकिन इस पल ज़िद्दी बच्चे की तरह बार-बार आंचल खींचकर तुम मुझे परेशान करने पर तुले हो.
मेरी हर मुद्रा, हर एक्शन को तुमने फ्रेम में जड़ दिया है और एक बार फिर मैं सशंकित हो उठी हे कि कि तुम्हारी यह मोहाविष्ट वाणी कहीं भ्रम तो नहीं. मेरी भोली मासूमियत को उन्हीं पूर्वाग्रहों के शिकंजों में तो नहीं कस रही, जिनको मैं अब तक स्वयं अपने इर्द-गिर्द कसती रही थी और शायद इसीलिए मैं कभी भी उन घनेरे क्षणों को पूरी तरह जी नहीं पाई. कभी भी तो नहीं भूली मैं वह दिन, जब तुम पहली बार अचानक एक गंधर्व पुरुष से सामने आ खडे हुए थे. मगर मुझे सचमुच तुम्हारी ज़रूरत थी. मैं अपनी महत्वाकांक्षाओं के हिंडोले में बैठी हुई ऊंची पींगे भरने के लिए तुम्हारे शब्दों का, तुम्हारी चिन्तनाओं का सहारा चाहती थी. एक सतही पारदर्शीं धरातल पर मैं अपना ही स्वार्थ लिए अपने ही बसंत में मगन थी.
कभी-कभी चौंक भी उठती थी कि आखिर यह सब तुम किस मोह से, किस आकर्षण से बंधकर आत्मदान दिए जा रहे थे. शिमला की बर्फीली पहाड़ियों से बेख़बर अपने ही कमरे में बंद हर रोज़ मुझे एक ही आहट का इंतज़ार रहता था और सचमुच तुम हर रोज़ घड़ी की सुइयों से बंधे-बंधे द्वार पर दस्तक दिया करते. तुम आते, कुर्सी में धंस जाते और म्यूज़िक ऑन कर देते. कमरे में फैली हल्की नीली रोशनी में मद्धम संगीत की स्वर लहरियां तैरती रहतीं और कमरे के एक कोने में तुम और दूसरे कोने से सटी मैं घंटों गीतों के बोल और उनके पीछे छिपे दर्द और ख़ुशी के एहसास को पीते रहते.
ग़ज़लों के कैसेट्स तुम्हें बहुत पसंद थे. कभी-कभी तुम ढेर सी किताबें ले आते थे मेरे पढ़ने के लिए. और जब एक बार किसी विषय पर बहस छिड़ जाती, तो चाय का प्याला ठंडा होता रहता और ख़ामोशी से हमारी बातें सुनता रहता. तुम बीच-बीच में कहीं खो जाते या अक्सर कुछ क्षणों के लिए मेरे चेहरे को घूरने लगते. मेरी वह मस्ती, मेरा वह आत्मविस्मरण पल भर में बिला जाता और मैं सहज होने की प्रक्रिया में बुहत असहज हो जाती.
एक दिन तुम नियत समय पर नहीं आए थे. उस दिन मैंने तुम्हारे साथ खाना खाने का विचार किया था. फिर अचानक मेरी भूख मर गई थी. जाने क्या हुआ कि दूसरे दिन भी तुम नहीं आए और उस दिन जाने किस अन्त:प्रेरणा से प्रतीक्षा की बन्दनवार सी मेरी डायरी में कविताएं सज गईं. तीसरे दिन तुम आए, तो मैं समझ ही नहीं पाई कि तुम्हारा स्वागत कैसे करूं? अपने मन को स्वयं ही छलते हुए मुझे यह महसूस होने लग गया था कि असहज होने की प्रक्रिया निरन्तर बढ़ती जा रही है और मनु मेरे जीवन की महत्वाकांक्षाओं और जिजीविषा के रस के लिए अनिवार्य बनता जा रहा है. अचानक लगा जैसे पूर्णिमा के दिन सागर में ज्वार आता है, ऐसे ही उसने मुझे पूर्णिमा मान लिया था. मेरी सारी सीमाओं को विस्तार दे दिया था.
मेरी हठधर्मिता और अहं किसी घनेरी छांव में पालतू खरगोश सा दुबक गया था. मित्रता का यह सहज व्यापार मन-प्राणों में पुलक बन समा गया था. कभी ऐसा होता कि झटके से तुम खड़े हो जाते और मोहाविष्ट सी मैं अनजाने ही… तुम्हें सुन लेती और दोनों बाहर निकल पड़ते. कितनी ही देर हम चुपचाप बर्फ़ रहते. चारों तरफ़ की सर्दीली ख़ामोशी को रौंदते हमें भीतर ही भीतर गुदगुदाती रहती. बिना बोले ढेरों बातें कह लेते, सुन लेते. अगर टेपरिकार्डर ईज़ाद हो चुका होता, जो बिना बोले दिल की धड़कनों के संगीत को टेप कर सकता, तो शायद दुनिया बेहतरीन नायाब संगीत समय नक़्श हो गया होता. सुरमई उस अंधेरे की गुलाबी खुनक में दूर-दूर तक की झपझपाती रोशनियां मुस्कुरा कर हमारा स्वागत कर रही होतीं और हम अपनी ही दासतां में गुम लौट आते.
मेरे दरवाज़े पर तुम ठिठकते और हाथ को हौले से दबाकर तुम लौट पड़ते. 'न कोई बेचैनी, न कोई बेबसी बस… राहे कदम में सज़दा करती निगाहें शब-अ-खैर कह जातीं. मैंने अपनी यादों के झरोखों को फिर से झाड़-पोंछ लिया है. उठकर एक ग्लास ठंडा पानी पिया और एक मस्त अंगड़ाई लेकर खिड़की पर जा खड़ी हुई. सामने फैली नीली झील अपने पूरे विस्तार से आमन्त्रित करती प्रतीत होती है.
शाम की इस सांवली छाया में दूर जा रहे स्टीमर में केवल एक लड़की लाल ब्लाउज़ और काली जीन्स में अकेली बैठी हुई है. ताज्जुब है, पश्चिमी देश के इस महानगर में, इस समय कोई लड़की इस छलकती उम्र में जाने किन ख़्यालों में खोई है.
सच ही तो है, निषेध न होने पर अधिक रस ग्रहण नहीं किया जा सकता. या हो सकता है, यह भी मेरी तरह किन्हीं स्मृतियों से लिपटी है. मैं छह वर्षों से यहां रहते हुए भी यह नहीं समझ पाई कि भारतीय संस्कारों की संवेदनाएं, जो केवल शरीर-विज्ञान से नहीं जुड़ी हैं वे यहां के मनोविज्ञान में भी पनप सकती हैं या नहीं. लेकिन इतना निश्चित है कि पश्चिमी सभ्यता का यह खुलापन भारतीय दिमाग़ों में ज़रूर घर बनाता जा रहा है. बहरहाल… अचानक तुम्हारा खीझा हुआ स्वर मेरे कानों से टकराने लगा है. तुम्हारा समूचा वजूद मुझे अपनी उपस्थिति से झकझोरता सा प्रतीत हो रहा है.
"नीलू, मैं तुम्हारे घिसे-पिटे आदर्शवाद से तंग चुका हूं. मेरे पीछे तुम मेरी यादों में डूबी रहती हो और मेरे सामने तुम स्वयं को एकदम समेट लेती हो."
मैं चौंक कर तुम्हें देखने लगी. तुम्हारा टोन मुझे कुछ बदला सा लग रहा और तुम्हारी नज़रें मेरे कंधों से पार कुछ खोजती सी लग रही हैं. मैं अचानक अकारण सजग हो उठी हूं और साड़ी का आंचल अपने गिर्द लपेट लिया है. पता नहीं क्यों, तुम्हारी दृष्टि का सामना नहीं कर पाती और उठ आती हूं.
गैस पर चाय का पानी चढ़ाती हूं, पर फिर भी पानी खौलने तक रसोई में ही खड़ी रहती हूं. चाय के प्याले लेकर जब मैं पहुंचती हूं, तब तक तुम सहज कैनवास पर रेखाएं उकेर रहे थे. मैं तुम्हारे पास बैठ गई थी और तुम्हें चित्र बनाते हुए देखने लगी थी. कैनवास पर धड़ से ऊपर गर्दन एक चेहरा अंकित किया था तुमने. दो आंखें, नुकीली नाक और कुछ कांपते से अधर. बिखरी हुई केशराशि, जिसकी अस्त-व्यस्त एक-दो लटें माथे पर झुलती हुई. तुम्हारा वह ध्यानावस्थित तन्मय रूप ही मेरी सबसे दुर्बलता थी. उस एकाग्रता में बिना कोई आहट किए मैं खो जाती थी. जब तक तुम सिर ऊपर उठाते, चाय की प्यालियों पर कई परतें मलाई की जम चुकी होती थीं. मैं अपराधी सी और चाय बना लाने के लिए उठती, तो हौले से हाथ पकड़ कर मुझे बिठा देते और बड़े तृप्त भाव से चम्मच से मलाई उतारकर ठंडी होती हुई चाय सिप करने लगते.
मैं अक्सर आत्मविस्मृत होकर मुग्ध भाव से तुम्हें देखती रहती, पर मनु इसी भोली प्रक्रिया में एक दिन तुम्हारी आंखों का रंग बदलने लगा था. चाय पीते-पीते उनमें मदिर डोरे तैरने लगे थे और तुम्हारी दृष्टि ने मुझे भीतर तक खींच लिया था. तुम्हारे होंठों की थिरकन कोई रस खींचने के लिए बेताब हो उठी थी और मैं जबरन बांह छुड़ाकर वहां से भाग गई थी. तुम्हारे आहत दर्प को यह गवारा न हुआ और ताव खाया पौरुष फनफनाकर दरवाज़े के बाहर हो गया था.
मुझे याद है, मैं दौड़कर बाहर आई थी, पर तुम लम्बे-लम्बे डग भरते हुए हवा से लड़ते हुए, अंधेरों में खो गए थे और फिर तुम पूरे छह दिन तक नहीं आए थे. मैं, जो रोज़ पहले कॉलेज से तुमसे मिलने की उत्कंठा में लौटती थी, अब रोज़ शाम को रोशनियों से लड़ती हुई अकेली हर आहट का जायज़ा लिया करती थी. मैंने बाहर जाना विल्कुल बंद कर दिया. खिड़कियों के मोटे परदे गिरा दिए थे. बाहर के नज़ारे मुझसे रूठने लगे थे. तुम्हारी यादों को मैंने खरोंच-खरोंच कर मिटाना चाहा था, पर वे तो शैवाल सी मेरे तन-मन से लिपट गई थीं.
और फिर एक दिन अख़बार में मैंने अग्रिम अध्ययन के लिए यहां का विज्ञापन पढ़ा. अपने मोह की प्रतिक्रिया में मैंने फॉर्म लेकर भर दिया. तुम्हारा वह आक्रामक रूप मुझे रास न आया था. मुझे लगा स्नेह के रस-निर्झर में यदि वासना का काला रंग घुलने लगता है, तो स्नेह के सड़ने की प्रक्रिया जारी हो जाती है और मुझे यह कतई गवारा न था. मैं भी कुछ कठोर हो चली थी. किन्तु पूरे छह दिन बाद तुमने जब दरवाज़े की घंटी बजाई और मैंने तुम्हें देखा, तो लगा बीच के अंतराल का कहीं कोई नामोनिशां न था. तुम वैसे ही सहज और आत्मीय लग रहे थे, जैसे रोज़ मिलते रहे थे. मुझे तुमने रूठने का, खीझने का मौक़ा भी न दिया.
कमरे में अंधेरा घिर आया था. खिड़की के पार दूर-दूर चमकती रोशनियां झील में झिलमिला उठी थीं, मगर कमरे के कल्ई अंधेरे में मेरी यादों का सुनहरापन कण-कण होकर झरने लगा था. बीच की सारी दूरी, वक़्त का लम्बा साया किसी जादुई चमत्कार सा हट गया था. दिशाएं थम गई थीं, मगर दिल की धड़कनें एक सुर, लय, ताल में बंधी गतिशील थीं. धीर-धीरे मौसम रंग बदलने लगा था. मौसम हमेशा बदलता है, व्यक्ति के मन का भी और बाहर का भी, मैं ही भूल गई थी. तुम्हारा धैर्य चुकने लगा था और अत्यधिक मिठास तत्ख लगने लगी थी.
यह भी पढ़ें: पहला अफेयर: वो ख़त जो कभी न गया (Pahla Affair: Wo Khat Jo Kabhi Na Gaya)
मनु, कैसे भूल सकती हूं वह दिन.. वही दिन जो आज तक मेरी आंखों के कोरों में बिना हिले-डुले टंगा हुआ है. उस दिन जब तुम आए थे, काफ़ी भरे-भरे से थे, लगा था सारी महत्वाकांक्षाएं और भविष्य के अनिश्चित अब भी कहीं दुबक गए है या ख़ुशी से मदहोश हो अपना आपा भूल चुके हैं. अचानक तुमने मुझे अपने हॉस्टल चलने के लिए ज़ोर दे डाला था. मुझे बाहर जाना गवारा न था. समूची सहजता के बावजूद मैं कहीं औपचारिक भी थी, "मैं अपनी सीमाओं में चिर हूं…" अक्सर कहा करती थी, पर हमेशा तुम मुस्कुरा कर उड़ा दिया करते थे.
उस दिन दिनभर बर्फ़ गिरने के बाद शाम को मौसम बहुत सुहावना हो गया था. कमरे में जलती हुई अंगीठी की लौ ढेर सारे काले बादलों के बीच चमकती हुई बिजली सी चमक रही थी. सांसों में कोई मीठी धुन बंसी की टेर सी महसूस हो रही थी. ऐसे में मेरी "अपनी सीमाओं में चिर…" होने की बात तुम्हें ऐसी ही प्रतीत हुई थी, जैसे मीठी रागिनी बजते-बजते वीणा का कोई तार झन्न से टूट गया हो. तुम समस्त मोहबंध को झटके से तोड़कर बाहर चल दिए थे और मैं उस दिन चाहकर भी तुम्हें पुकार न सकी थी. मेरी आंखों में गीले बादलों के साये तैर आए थे, मगर मुझे विश्वास था… तुम अकेले रह न पाओगे तुम ज़रुर आओगे जैसा कि अक्सर होता था. और फिर धीरे-धीरे दिन लम्बे होते गए. रातों के साये गहराते रहे और मेरा विश्वास चटकता चला गया. चटके दर्पण में अतीत की परछाइयां लिए हुए.
इसी बीच मुझे दिल्ली से इंटरव्यू के लिए बुलावा आया. मैं तुमसे मिलना चाहती थी. तुम्हारे हॉस्टल गई, तो पता लगा तुम जा चुके थे बिना मुझे बताए, बिना मुझसे मिले. मुझे सिर्फ़ यही मालूम था कि तुम्हारा घर दिल्ली में हैं बस. मैं दिल्ली इंटरव्यू के लिए गई थी. बाद में दो दिन दिल्ली की सड़कें छानती रही, पर सब व्यर्थ.
अब शिमला मेरे लिए शिमला न रह गया था… वह कमरा, वे किताबें, वे रंग और कैनवास और अधूरे रेखाचित्र… मुझसे देखे न जाते थे. कुछ दिनों बाद मुझे यहां की ऑफर मिल गई और बाद के दो महीने मुझे यहां की तैयारी और ज़रूरी औपचारिकताएं पूरी करने में लग गए.
मैं कैसे कहूं कि वक़्त के पत्थरों के नीचे ढका यादों का झरना हर वक़्त मेरी नसों में बहता रहा. यहां आने के बाद ही मैं कुछ व्यवस्थित हुई और ज़िंदगी की किताब का अगला अध्याय वक़्त ने लिखना शुरू कर दिया. मैं झूठ नहीं कहूंगी तुम्हारी यादें अक्सर टिपटिपाती टीस की तरह मुझे काफ़ी अर्से तक कचोटती रही हैं, मगर साथ ही सब्ज़ी में अधिक डाले गए नमक के स्वाद की भांति तिलमिलती भी रही हैं. तुमने मुझे नहीं समझा तुमने उस मधुरता के उदात्त रूप को नहीं समझा. फिर भी अब मैंने उस मिठास को ही संजो लिया है, जिसने मुझे ज़िंदगी का वह रस दे दिया था, जिसे नीलू उम्रभर का पाथेय बना सकती है. आज भी तुम मेरे पास हो, हर वक़्त पास रहते हो, तुम्हीं तो मुझे यहां तक लाए हो.
- सुदेश बत्रा
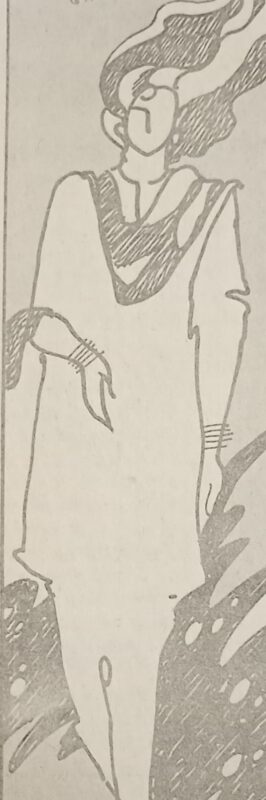
अधिक कहानियां/शॉर्ट स्टोरीज़ के लिए यहां क्लिक करें – SHORT STORIES


