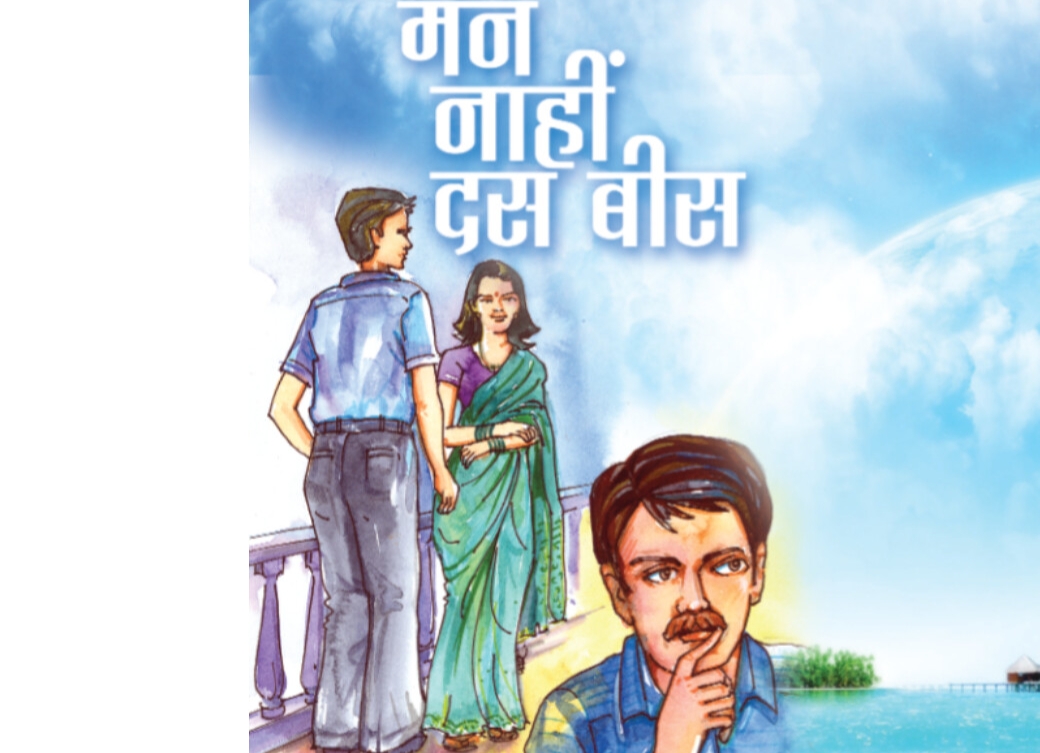दैहिक स्तर से अलग था हमारा रिश्ता और ऐसे ही रहेगा. जिस शिद्दत से मैंने पहले उसे चाहा था, वैसे ही आगे भी चाहता रहूंगा. पाबंदियां तो शारीरिक प्रेम पर ही हो सकती हैं. मन से जुड़ा रिश्ता कौन तोड़ सकता है. कौन-सा समाज मर्यादित कर सकता है? पर भविष्य में कभी उससे मिलूंगा नहीं, यह भी निश्चित है. इसलिए न तो मैंने उसके घर का पता पूछा और न ही फोन नंबर लिया.
हमारे सीनियर मेहता साहब के विवाह की रजत जयंती है और पार्टी में ऑफ़िस के अनेक साथी आमंत्रित हैं. विवाह अथवा विवाह संबंधी किसी भी अवसर में शामिल होना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, पर मन की इच्छा-अनिच्छा एक और बात है और व्यावहारिकता निभाना दूसरी. फिर मेरा परम मित्र पारिख मुझे ऐसे कहां छोड़ने वाला था, जिसने मुझ जैसे बेवकूफ़ को दुनियादारी सिखाने की पूरी ज़िम्मेदारी ले रखी है. उपहार भी उसी ने दिलवा दिया और संग ले भी गया.
द़फ़्तर के सहकर्मियों के अलावा मेहता दम्पति के सगे-संबंधी और अन्य मित्रगण थे. तरह-तरह के पकवानों और पेय पदार्थों से मेजें सजी हुई थीं. कुछ लोग मिलने-मिलाने के इरादे से जाते हैं ऐसे मौक़ों पर, तो कुछ बढ़िया भोजन के निमित्त. मेरी इन दोनों में ही रुचि नहीं थी. मेरा बस चलता तो उपहार पकड़ा कर चुपचाप खिसक लेता.
कहीं भी नहीं लगता आजकल मेरा मन. शरीर घर-द़फ़्तर के सारे कर्त्तव्य निभाता चलता है, पर मन तो जैसे काष्ठ हो गया है. एक अजब, उचाट-सी वीरानगी समा गई है मन के भीतर. मैं एक किनारे खड़ा, झुंझलाया-सा, पारिख दम्पत्ति के लौट चलने की प्रतीक्षा कर रहा था कि मुझे वसुधा दिखाई दी.
एक बार तो मुझे लगा कि यह मेरा कोरा वहम् है. मुझे तो हर जगह और हर समय वसुधा ही दिखाई देती है, पर फिर भी अपना संशय दूर करने के लिए मैं उधर ही चल पड़ा. वह अपनी किसी परिचिता से बातें करने में मशगूल थी. आज वह संपूर्ण युवती लग रही थी. किशोरावस्था में वह मेरी अभिन्न मित्र थी, लेकिन आज कहीं बहुत पीछे छूट चुकी है. अवसर के अनुकूल उसने हल्के काम वाली साड़ी पहनी हुई थी. थोड़ा-सा शृंगार भी था. कितनी बदल-सी गई थी वह. पर अभी भी कुछ था, जो उसे अतीत से जोड़ता था. वह सम्मोहक मुस्कुराहट, आंखों में वही स्नेहिल, विश्वसनीय भाव. बहुत कुछ बदल कर भी तो वह मेरी वसुधा ही थी. कुछ देर मैं उसे थोड़ी दूर से देखता रहा, फिर उसके पास जाकर खड़ा हो गया चुपचाप. उसने नज़र उठा कर देखा और पहचानते ही अचकचा गई. अब तो संदेह की कोई गुंजाइश भी नहीं बची थी.
यह भी पढ़ें: प्यार में क्या चाहते हैं स्री-पुरुष? (Love Life: What Men Desire, What Women Desire)
एक बार तो जी चाहा उसका हाथ कस कर अपनी मुट्ठियों में पकड़ लूं, पर बुद्धि ने अपना क्रोध याद दिलाया, उसकी बेवफ़ाई याद दिलाई. अब वह किसी की पत्नी है. मेरा कोई हक़ नहीं बचा था उस पर. हालचाल भी क्या पूछता? अच्छी-भली तो लग रही थी. असमंजस की स्थिति में कुछ पल खड़ा रहा और फिर चलने को हुआ तो वह मेरा इरादा भांप कर बोली, “क्या मैं कल थोड़ी देर के लिए तुमसे मिल सकती हूं?” मेरी प्रतिक्रिया पढ़ने के लिए उसने एक आशाभरी निगाह मुझ पर डाली. पर मैंने मिलने की कोई उत्सुकता नहीं दिखाई. तटस्थ ही रहा और अपना कार्ड पकड़ा कर लौट आया, बिना एक भी शब्द उससे कहे.
रात को नींद कहां से आती. न चाहते हुए भी विगत बार-बार स्वयं को दोहराता रहा. आज क़रीब 15 साल के बाद देखा था वसुधा को, जिसमें से पहले 5 साल तो उम्मीदों से भरपूर ही बीते थे और फिर उम्मीदें बिखर गईं तो शेष अवसाद और हताशा में डूबे बीते. सुनहरे भविष्य के ख़्वाब बुनना ज़िंदगी का एक हसीन हिस्सा होता है और मैंने तो कोई ऐसा ख़्वाब भी नहीं देखा था, जिसके कि पूरा होने की कोई संभावना न होती. पर शायद सपनों की नियति ही है टूटकर बिखर जाना. सब सपने यदि पूरे हो जाते तो वे स्वप्न ही क्यों कहलाते?
दस वर्ष पहले की वह रेल यात्रा आज भी ताज़ा है मेरी स्मृति में. गाड़ी की एक सुर आवाज़, हिचकोले लेती चाल, लोगों की आवाजाही, आज भी आंख बंद करके मैं सब कुछ देख-सुन सकता हूं. अपनी शिक्षा पूरी कर ढेर-सी उमंगें मन में लिए मैं जमशेदपुर लौट रहा था. अपना जन्म स्थान सभी के लिए प्रिय होता है. मेरा जन्म स्थान तो सुंदर भी था. खुली-चौड़ी सड़कें, साफ़-सुथरी और हरियाली से भरपूर. एक आदर्श शहर के मॉडल-सा, छोटा-सा आधुनिक शहर. बस, एक ही मुश्किल थी, उच्च शिक्षा की कमी. स्कूली शिक्षा पूरी होते ही आगे की पढ़ाई के लिए हमें अपना शहर छोड़ना पड़ता था.
पर असल बात तो मैंने आपको बताई ही नहीं. क्यों मैं इस क़दर बेक़रार हो रहा था जल्द से जल्द जमशेदपुर पहुंचने के लिए? वहीं तो वसुधा रहती थी, जिसके कारण मेरा मन गाड़ी पहुंचने से पहले ही वहां के अनेक चक्कर लगा आया था. निर्भर तो मेरा शरीर था गाड़ी के गंतव्य तक पहुंचने के लिए, उन्मुक्त मन को न दूरी बांध सकती है, न देरी. हर बार एक नई कल्पना के साथ उड़ान भरता वह. जिस तरह मैं उतावला हो रहा हूं वसुधा से मिलने के लिए, उसी तरह वह भी तो मेरा इंतज़ार करती होगी. और मुझे यूं अचानक सामने पा उसके आंसू ही निकल आएंगे मारे ख़ुशी के. कभी देखता कि वह घर पर नहीं है और मैं उसके ही घर बैठा उसके लौटने का इंतज़ार कर रहा हूं. कुर्सी पर बैठा मैं उसकी मां से गप्पे लड़ा रहा हूं. बीते 5 वर्ष का हालचाल बांट रहा हूं. कभी कल्पना करता कि उसे सामने पा स्वयं को रोक नहीं पाया हूं और उसके दोनों कंधों को पकड़ देर तक उसे निहारता खड़ा रह गया हूं. अंतिम बात सोच मैं ख़ुद ही सकपका गया. अनजाने में भले ही कभी मेरा हाथ उसे छू गया हो अन्यथा जान-बूझकर उसे छूने का कभी प्रयास भी नहीं किया. सहशिक्षा होने के बावजूद स्कूल का कड़ा अनुशासन और हमारे घरों के संस्कार. माहौल भी आज की तरह खुला नहीं था तब. मुंबई में रहकर मैं कुछ बोल्ड हो गया था या फिर आत्मविश्वासी या शायद दोनों ही बातें सही थीं.
वसुधा से मैं एक क्लास आगे था. पर हम चार छात्रों का एक ग्रुप था, जो एक ही दिशा में घर होने के कारण संग ही आते-जाते थे. वसुधा से मेरी दोस्ती दिन-प्रतिदिन बढ़ती गई. मेरे पिता के असमय निधन के बाद परिवार में मैं और मां ही रह गए थे, पर अब वसुधा भी उसका हिस्सा बनती जा रही थी. ज़ाहिर तौर पर कुछ नहीं कहा गया था, पर अनकहा बहुत कुछ था. भविष्य की अनेक योजनाएं बनाया करते थे हम और इन सबमें मां की मौन स्वीकृति भी शामिल थी.
वसुधा के माता-पिता भी अनभिज्ञ नहीं थे हमारे रिश्ते से और मुझे उनका भरपूर स्नेह प्राप्त था. बस, मेरे अपने पैरों पर खड़े होने का इंतज़ार था सब को. मुझे मुंबई इंजीनियरिंग कॉलेज में दाख़िला मिल गया था. मां अकेली जमशेदपुर रह कर क्या करती? अतः वह भी मेरे संग आ गई और हम मुंबई में कमरा लेकर रहने लगे.
वसुधा के पिता कार मैकेनिक थे. अपने वर्कशॉप से उन्हें इतनी आमदनी हो जाती थी कि तीन जन का उनका परिवार सम्मानपूर्वक ज़िंदगी बसर कर सके.
मुंबई में रहते हुए प्रथम दो-ढाई वर्ष तो वसुधा से नियमित पत्र-व्यवहार चलता रहा. लेकिन धीरे-धीरे उसके पत्रों का सिलसिला धीमा पड़ने लगा. आते भी तो, जल्दबाज़ी में लिखी चंद पंक्तियां ही होतीं, जिनमें एक-दो बार उसके पिता के अस्वस्थ रहने का ज़िक्र भी था, पर मेरे पूछने पर उसने उत्तर में ‘सब ठीक है’ ही लिखा था.
मेरी शिक्षा पूरी हुई और जल्द ही नौकरी मिलने की संभावना थी. यह सोचकर कि वसुधा अपने माता-पिता से बहुत दूर नहीं जाना चाहेगी, मैंने भारत के उत्तरीय प्रांतों की नौकरियों के ही आवेदन-पत्र भरे. अब समय आ गया था कि वसुधा को पाने का अपना सपना पूरा कर सकूं.
जब मैं उसके घर पहुंचा, तो सांझ घिर आई थी. मकान तो वही था, पर द्वार किसी अपरिचित ने खोला और बताया कि वह पिछले एक साल से वहां रह रहे हैं. पुराने मालिकों का नया पता नहीं था उनके पास. अधिकांश मित्र भी तितर-बितर हो चुके थे, पर उनके परिवार वहीं थे. उन्हीं में से एक से पता चला कि वसुधा एवं उसके माता-पिता जमशेदपुर छोड़ गए हैं और सुना है वसुधा का विवाह भी हो गया है.
मुझे लगा मानो पूरा शहर ही मेरी खिल्ली उड़ा रहा है. यह बात भी तो गले नहीं उतर रही थी कि वसुधा के माता-पिता ने जबरदस्ती ही उसका विवाह अन्यत्र कर दिया होगा. वहां रुकने का कोई कारण शेष नहीं बचा था. पराया ही हो गया था मेरा अपना शहर मेरे लिए. मैं मुंबई लौट आया. एक-दो जगह नौकरी करने के बाद कलकत्ता की एक बड़ी फर्म में मुझे नौकरी मिल गई और मैं मां के साथ यहीं बस गया.
नदी के प्रवाह की मानिंद ही होती है काल की गति. समय भी जब आगे बढ़ता है, तो बहुत कुछ चाहा-अनचाहा अपने किनारों पर छोड़ता चलता है, ठीक नदी की ही तरह. ज़िंदगी की त्रासदी तब होती है जब अपना कोई बहुत प्रिय, बहुत निजी किनारे पर छूट जाता है. पर ज़िंदगी को तो आगे बढ़ना ही होता है, पीड़ा और टीस मन में समेटे. भीड़ में भी एकाकी होने का श्राप ढोते हुए, पर एक फ़र्क़ है दोनों में. नदी मुड़ती है, राह बदलती है तो शनैः शनैः, जबकि जीवन में एक पल, एक ही घटना किसी ऐसे मोड़ पर ला पटकती है कि सब कुछ बेमानी हो जाता है.
बहुत कोशिश की मैंने वसुधा को भुलाने की. अपने समूचे अतीत को दिलो-दिमाग़ से मिटाने की, पर कुछ बालहठ ही होता है ऐसे पलों का, यादों में डटे रहने का. तभी तो आज उसे देख घाव फिर टीसने लगा था.
दूसरे दिन सुबह ही वसुधा का फ़ोन आया और वह लंच के समय द़फ़्तर आ गई. हो सकता है उसने सोचा हो कि वह मुझे कहीं बुलाए तो मैं जाऊं या न जाऊं. बहरहाल, वह मेरे सामने थी और हम कैंटीन के शोर-शराबे में न बैठ, बाहर पार्क की ओर निकल गए.
मेरे भीतर वसुधा के प्रति क्रोध से अधिक निराशा का भाव ही रहा है और वह ज़रूर यह बात समझ चुकी थी. यह भी जानती थी कि शब्दों के इस्तेमाल में मैं थोड़ा कृपण हूं. अतः कुछ देर की ख़ामोशी सहन कर उसने स्वयं ही बात छेड़ी,
“कारण भी नहीं पूछोगे. बस यूं ही नाराज़ बैठे रहोगे मुझसे?”
“अब क्या फ़र्क़ पड़ता है?” बस इतना ही कह पाया मैं.
“तुम्हें न पड़े पर मुझे तो पड़ता ही है. तुम ने तो यह मान लिया कि मैंने तुम्हारे साथ धोखा किया. कुछ पूछते, तभी जान पाते कि मुझे स्वयं से कितना संघर्ष करना पड़ा था निर्णय लेते समय.”
वसुधा बीते वर्षों का ब्योरा देने लगी. वह बताती रही, मैं सुनता रहा.
“तुम्हें मैंने एक बार लिखा था कि पापा की तबीयत ठीक नहीं चल रही है. शुरू में तो मामूली बीमारी समझ इलाज करवाया, पर कोई फ़र्क़ नहीं पड़ा. जब टेस्ट कराए गए, तो डॉक्टरों ने बीमारी का नाम एस.एल.ई. बताया, जो पापा की किडनी पर असर कर रही थी. यूं भी देर से पकड़ में आती है यह बीमारी, फिर अधिकांश तौर पर स्त्रियों को ही होने के कारण डॉक्टरों का ध्यान पहले इस ओर गया ही नहीं. जब पक्का हो गया कि एस.एल.ई. बीमारी ही है, तो डॉक्टर ने फौरन कलकत्ता ले जाने को कहा. तुम्हें ये सब नहीं लिखा, ताकि तुम्हारी पढ़ाई में कोई रुकावट न आए और तुम एकचित्त होकर अपनी पढ़ाई कर सको.
यह भी पढ़े: पुरुष होने के भी हैं साइड इफेक्ट्स (7 Side effects of being men)
जमशेदपुर में ही एक बार जब मैं पापा को लेकर अस्पताल गई थी तो वहां मनीष से मुलाक़ात हुई. याद होगा तुम्हें मनीष. तुम से दो क्लास सीनियर था. एक ही स्कूल में पढ़े होने के कारण कुछ जान-पहचान तो थी हमारे बीच. मुझे परेशान देख वह कारण पूछने लगा. उसने हमारी बहुत सहायता की. पापा को अस्पताल लाने-ले जाने, दवा का इंतज़ाम इत्यादि सारी ज़िम्मेदारी उसने ले ली. वर्कशॉप का काम भी देखने लगा, ताकि रुपए-पैसे के कारण इलाज न रुके. और जब पापा को कलकत्ता ले आए, तो सप्ताहांत में कलकत्ता का चक्कर भी लगा जाता. अपनी तरफ़ से मां और मैं भी पूरा प्रयत्न कर रहे थे. मनीष भागदौड़ के सारे काम निबटा जाता और सलाह-मशविरा भी हो जाता.
जब लगा कि पापा को अभी लंबे समय तक डॉक्टरों की निगरानी में कलकत्ता ही रहना पड़ेगा और उसके बाद भी वह वर्कशॉप का काम नहीं संभाल पाएंगे तो उनके कहने पर मनीष ने वर्कशॉप का काम समेट पूंजी ऐसे व्यापार में लगा दी कि नियमित आमदनी होती रहे. बिजली के उपकरणों का ख़ानदानी कारोबार था मनीष और उसके दो भाइयों का. उसी की एक ब्रांच उसने यहां कलकत्ता में ही खोल ली और यूं उसकी भागदौड़ भी कुछ कम हो गई.
उन तनाव भरे दिनों में मनीष का संबल तो रहा ही, मानसिक सहारा भी बहुत मिला. पापा तो अपनी हर ज़रूरत के लिए उस पर निर्भर रहने लगे थे. मां भी अपनी हर उलझन उससे बांट कर सलाह-मशविरा करती. हर रोज़ आने-जाने से वह घर के सदस्य सा ही बन गया था और ऐसे ही एक दिन उसने पापा से मुझसे विवाह करने की इच्छा ज़ाहिर की.
नहीं, मुझ पर दबाव किसी ने नहीं डाला था. मनीष न जानता हो तुम्हारे बारे में, मम्मी-पापा तो जानते ही थे. अतः उन्होंने निर्णय पूरी तरह से मुझ पर ही छोड़ दिया. मनीष ने सहायता किसी पूर्व योजना के तहत की थी, यह सोचना भी निराधार है. दूसरों की सहायता करना उसका स्वभाव ही है. किसी को भी संकट में देख वह पूरी सहायता करता है आज भी. दरअसल, वह इन दिनों भी अपने छोटे भाई के साथ उसके किसी निजी काम से गया हुआ है. ऐसे ही जब उसने हमें परेशानी में देख सहायता का हाथ बढ़ाया था, तो बीच मझधार में नहीं छोड़ पाया था.
यदि उसने दबाव डाला होता, अपने उपकारों का सिला मांगा होता, तो मेरे लिए मना करना आसान होता. पर उसने तो मात्र अपनी चाहत जताई थी, इच्छा ज़ाहिर की थी बस. वह एक प्रार्थी की तरह खड़ा था जबकि मैं ही उसके उपकारों तले दबी थी. हमारे ही कारण वह अपना परिवार छोड़ यहां अकेला रह रहा था. मैं उसकी अच्छाइयों के आगे विवश हो गई थी सरू. ‘हां’ करने के अलावा किसी तरह उसके उपकारों का सिला नहीं चुका सकती थी मैं.”
वसुधा अपनी बात पूरी करके जा चुकी है. मैं उसे स्वयं ऑटो में बिठा कर विदा कर आया हूं और लौट कर पार्क की उसी बेंच पर बैठा हूं. न तो द़फ़्तर लौटने का मन है और न ही घर जाने का. इस बेंच पर उसके बैठे होने का एहसास अभी बाकी है. मैं इस एहसास को अभी कुछ देर और जी लेना चाहता हूं. यह एहसास फिर कभी नहीं मिलेगा मुझे, यह जानता हूं मैं. जीवन में चाहा हुआ सब मिल जाए, ऐसा किस के साथ हुआ है? मैं नियतिवादी नहीं, पर सत्य को स्वीकारना आता है मुझे.
वसुधा पर जो थोड़ा-सा रोष बाकी था, वह समाप्त हो चुका है. दैहिक स्तर से अलग था हमारा रिश्ता और ऐसे ही रहेगा. जिस शिद्दत से मैंने पहले उसे चाहा था, वैसे ही आगे भी चाहता रहूंगा. पाबंदियां तो शारीरिक प्रेम पर ही हो सकती हैं. मन से जुड़ा रिश्ता कौन तोड़ सकता है. कौन-सा समाज मर्यादित कर सकता है? पर भविष्य में कभी उससे मिलूंगा नहीं, यह भी निश्चित है. इसलिए न तो मैंने उसके घर का पता पूछा और न ही फ़ोन नंबर लिया.
‘सरू’ मेरा असली नाम नहीं है. वसुधा ही ‘सरू’ कहकर छेड़ा करती थी मुझे, मेरे लंबे क़द के कारण और फिर यही प्यार का संबोधन बन गया था मेरे लिए. आज उसके मुख से मेरे असली नाम की बजाय फिर ‘सरू’ ही निकला था. उसके मन की अतल गहराइयों में आज भी मेरा वास है कहीं. यही संतोष बहुत है मेरे लिए.
रही बात मेरी, तो क्या स़िर्फ स्त्री ही एकनिष्ठ हो सकती है? गोपियों ने एक बात कही थी उद्धव से-
‘ऊधो! मन नाहीं दस बीस
एकहु तो सो गयौ श्याम संग…’
यही चिरंतन सत्य है. कम से कम मेरे लिए तो अवश्य ही. किसी और को पत्नी बनाकर मैं उसके साथ न्याय नहीं कर पाऊंगा. एक याद है, जो स्थाई रूप से मेरे संग है और उसी के साथ जीवन गुज़ारने की ठानी है मैंने.

अधिक कहानियां/शॉर्ट स्टोरीज़ के लिए यहां क्लिक करें – SHORT STORIES